महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग

गौतम बुद्ध
जैन धर्म की भाँति बोद्ध धर्म का भी अभ्युदय हिन्दु धर्म के विरोध में हुआ था | इसके आदि प्रवर्त्तक गौतम बुद्ध थे। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ई० पू० में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक बाटिका मे हुआ था। यह नेपाल की तराई में स्थित है। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम मायादेवी था। पिता कपिलवस्तु के क्षत्रिय राजा ये। ये गौतम गोत्र के थे, अतः सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। बचपन से ही सिद्धार्थ चिंतनशील प्रकृति के ये । कहा जाता है कि एक बार बचपन में ही वे रोगी तथा मृतक को पहली बार देखकर काँप गए थे तथा दुःख से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगे थे। वे एकान्त स्थान में बैठकर जीवन, मृत्यु और दुःख पर घंटों चिन्तन करने लगे । सिद्धार्थ की मनोवृति देखकर उनके पिता चिन्तित रहते थे।
उन्हें सांसारिकता की ओर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से उन्होंने
सिद्धार्थ का व्याह एक परम सुन्दरी कन्या यशोधरा के साथ करा दिया। यशोधरा रामग्राम के कोलियग्राम की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ ने लगभग 12 वर्षों तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इसी बीच उन्हें राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म की खबर पाकर सिद्धार्थ
को प्रसन्नता नहीं हुई। उनका हृदय और भी खिन्न हो उठा। जीवन- मरण और व्याधि- के दृश्य उनके हृदय को पीड़ा पहुँचाते रहे। अंततः एक रात सिद्धार्थ अपनी पली यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर मुक्ति-मार्ग की खोज के लिए निकल पड़े। इस घटना को ‘महाभि- निष्करमण’ कहते हैं । गृह-त्याग के पश्चात् सिद्धार्थ पाटलिपुत्र, राजगृह और गया गए । वहाँ उरुवेला नामक वन में इन्होंने घोर तपस्या की। यहाँ उन्हें मध्यम मार्ग अपनाने का ज्ञान मिला।

वे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे गए जहाँ साधना करते समय उन्हें शाश्वत ज्ञान मिला। अब सिद्धार्थ बुद्ध (ज्ञानी) हो गए । तत्पश्चात् उन्हें 35 वर्ष की आयु में एक वट वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान-प्राप्ति का स्थान बोधगया और पीपल का वृक्ष बोधिवृक्ष कहलाया। अब बुद्ध के मन में यह भावना आई, “मैं तो जागा, किन्तु अब मैं.जगत् को जगाऊँ, तभी मेरा जागना सार्थक है ”
विभिन्न कष्टों तथा दुःखों से पीड़ित प्राणी को ज्ञान व सत्य की शिक्षा देने वुद्ध निकल.पड़े। गया में उन्होंने तपस्सु और मल्लिक नामक दो बनजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी.बना लिया। गया से वे काशी के ऋषिपत्तन ( सारनाथ) नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने
अपना पहला उपदेश दिया और उन पाँच तपस्वियों को दीक्षा दी जिन्होंने उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया था। पाँचों तपस्वी अब उनके शिष्य बन गए। बौद्ध साहित्य में इसे ‘धर्म चक्र प्रवर्त्तन’ कहते हैं। फिर तो अनेक लोग बुद्ध के अनुयायी बनने लगे ।
उन्होंने अपनी शिष्य मंडली का एक संघ बनाया । अपने शिष्यों को बुद्ध ने उपदेश दिया,
भिक्षुओं! अब तुम लोग जाओ, भ्रमण करो, लोगों के हित के लिए । तुम में से कोई एक.साथ, न जाय । तुम लोग उस धर्म का प्रचार करो जो आदि मंगल है, मध्य मंगल है एवं अंत मंगल है।” बुद्ध ने परिव्राजक को कायाक्लेश और काम सुख अतिकिलमय अनुयोग और काम.सुखल्लक अनुयोग) से बचने का उपदेश दिया । उसे ‘मज्झिम पदिपदा’ (मध्यममार्ग) का अनुसरण करना चाहिए तथा ‘सत्य चतुष्टय ( चार आर्य सत्य ) का पालन करना चाहिए। संसार में दुःख है, दुःख के कारण हैं। इनसे मुक्ति मिल सकती है एवं इसके उपाय भी हैं। इसी को चार आर्य सत्य कहते हैं।
ये चार आर्य सत्य है।1.दुःख 2.दुख समुदाय 3. दुःख निरोध 4.दुःख निरोध मार्ग। इन्हें ही चत्वारिक आर्य सत्य कहा जाता हैं।
दुःख-निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग (अट्टांगिक मार्ग) हैं।
संभवत जैन धर्म की भाँति बोद्ध धर्म का भी अभ्युदय हिन्दु धर्म के विरोध में हुआ था | इसके आदि प्रवर्त्तक गौतम बुद्ध थे। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ई० पू० में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक बाटिका मे हुआ था। यह नेपाल की तराई में स्थित है। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम मायादेवी था। पिता कपिलवस्तु के क्षत्रिय राजा ये। ये गौतम गोत्र के थे, अतः सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। बचपन से ही सिद्धार्थ चिंतनशील प्रकृति के ये । कहा जाता है कि एक बार बचपन में ही वे रोगी तथा मृतक को पहली बार देखकर काँप गए थे तथा दुःख से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगे थे। वे एकान्त स्थान में बैठकर जीवन, मृत्यु और दुःख पर घंटों चिन्तन करने लगे । सिद्धार्थ की मनोवृति देखकर उनके पिता चिन्तित रहते थे।
उन्हें सांसारिकता की ओर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से उन्होंने
सिद्धार्थ का व्याह एक परम सुन्दरी कन्या यशोधरा के साथ करा दिया। यशोधरा रामग्राम के कोलियग्राम की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ ने लगभग 12 वर्षों तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इसी बीच उन्हें राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म की खबर पाकर सिद्धार्थ
क प्रसन्नता नहीं हुई। उनका हृदय और भी खिन्न हो उठा। जीवन- मरण और व्याधि- के दृश्य उनके हृदय को पीड़ा पहुँचाते रहे। अंततः एक रात सिद्धार्थ अपनी पली यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर मुक्ति-मार्ग की खोज के लिए निकल पड़े। इस घटना को ‘महाभि- निष्करमण’ कहते हैं । गृह-त्याग के पश्चात् सिद्धार्थ पाटलिपुत्र, राजगृह और गया गए । वहाँ उरुवेला नामक वन में इन्होंने घोर तपस्या की। यहाँ उन्हें मध्यम मार्ग अपनाने का ज्ञान मिला।
वे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे गए जहाँ साधना करते समय उन्हें शाश्वत ज्ञान मिला। अब सिद्धार्थ बुद्ध (ज्ञानी) हो गए । तत्पश्चात् उन्हें 35 वर्ष की आयु में एक वट वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान-प्राप्ति का स्थान बोधगया और पीपल का वृक्ष बोधिवृक्ष कहलाया। अब बुद्ध के मन में यह भावना आई, “मैं तो जागा, किन्तु अब मैं.जगत् को जगाऊँ, तभी मेरा जागना सार्थक है ”
विभिन्न कष्टों तथा दुःखों से पीड़ित प्राणी को ज्ञान व सत्य की शिक्षा देने वुद्ध निकल.पड़े। गया में उन्होंने तपस्सु और मल्लिक नामक दो बनजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी.बना लिया। गया से वे काशी के ऋषिपत्तन ( सारनाथ) नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने
अपना पहला उपदेश दिया और उन पाँच तपस्वियों को दीक्षा दी जिन्होंने उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया था। पाँचों तपस्वी अब उनके शिष्य बन गए। बौद्ध साहित्य में इसे ‘धर्म चक्र प्रवर्त्तन’ कहते हैं। फिर तो अनेक लोग बुद्ध के अनुयायी बनने लगे ।
उन्होंने अपनी शिष्य मंडली का एक संघ बनाया । अपने शिष्यों को बुद्ध ने उपदेश दिया,
भिक्षुओं! अब तुम लोग जाओ, भ्रमण करो, लोगों के हित के लिए । तुम में से कोई एक.साथ, न जाय । तुम लोग उस धर्म का प्रचार करो जो आदि मंगल है, मध्य मंगल है एवं अंत मंगल है।” बुद्ध ने परिव्राजक को कायाक्लेश और काम सुख अतिकिलमय अनुयोग और काम.सुखल्लक अनुयोग) से बचने का उपदेश दिया । उसे ‘मज्झिम पदिपदा’ (मध्यममार्ग) का अनुसरण करना चाहिए तथा ‘सत्य चतुष्टय ( चार आर्य सत्य ) का पालन करना चाहिए। संसार में दुःख है, दुःख के कारण हैं। इनसे मुक्ति मिल सकती है एवं इसके उपाय भी हैं। इसी को चार आर्य सत्य कहते हैं। ये चार आर्य सत्य है।1.दुःख 2.दुख समुदाय 3. दुःख निरोध 4.दुःख निरोध मार्ग। इन्हें व्है चत्वारिक आर्य सत्य कहा जाता हैं।
दुःख-निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग (अट्टांगिक मग्गा) हैं।
सम्यक् दृष्टि :
सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण ठीक हो। जैसा दृष्टिकोण होगा, वैसा ही हमारा काम होगा, तदनुरूप उसका परिणाम होगा।
सम्यक् संकल्प :
हमारे संकल्प ठीक हो। गलत काम करने का हम निश्चय न करें।
মमारे विचार पवित्र व शुद्ध हों।
सम्यक वाक्य :
हमारे वचन सही हो। बोलचाल ठीक नहीं रहने पर मनुष्य स्वयं तो दुखी रहता है, दूसरो को भी दुःख देता है।
सम्यक कर्म :
हमारे कार्य सम्यक् या सही हो। गलत काम करके हम मधुफल की आशा नहीं कर सकते।
सम्यक् आजीविका :
आजीविका से साधन ठीक हों। कोई अनैतिक आजीविका नहीं अपनाएँ।
सम्यक् चेष्टा :
हमारी चेष्टाएँ सही हों। कोई लाभ के लिए गलत काम नहीं करें।
सम्यक् स्मृति :
हमारी यादगारी सही रहे। स्मृति गलत रहने से हमारे विचार प्रभावित हो जाते हैं।
सम्यक् समाधि :
हमारा ध्यान सही हो। आध्यात्मिक चेतना सही हो।
दस शील :
बुद्ध ने नैतिक आचरण को शुद्ध एवं समुन्रत करने पर विशेष बल
दिया। इसके लिए उन्होंने दस शील के उपदेश दिए।
वे दस शील हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह ( संग्रह न करना), बह्मचर्य, नृत्य-संगीत का त्याग, सुगंधित व श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन, कोमल शय्या का त्याग एवं कामिनी-कंचन का त्याग।
इनमें प्रथम पाँच गृहस्थों के लिए आवश्यक थे, परन्तु संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के लिए सबका पालन अनिवार्य था।
बुद्ध. ने संसार में अपना संदेश फैलाकर मानवता को दुःख, शोक, मृत्यु. भय आदि से मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक मगध, सारनाथ आदि प्रदे्शों में घूम-घूम कर शिक्षा का प्रचार किया। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय
हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ई० पू० में कुशीनगर ( गोरखपुर ) में उनका देहान्त गया। यह घटना ‘महापरिनिर्वाण’ कहलाती, है।
यह दिलचस्प बात है कि (भारत में बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन भी हुआ। बुद्ध के उपदेश बहुत ही सरल थे। जीवन-संबंधी उनके दर्शन साधारण नियमों पर आधारित थे । ये सभी नियम युक्ति संगत एवं तर्क संगत थे। शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए सच्चरित्रता
और सदाचार पर बल दिया गया। बुद्ध का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनका हदय संसार के सभी दुःखी प्राणियों के लिए संवेदना एवं करुणा से परिपूरित था। बौद्ध धर्म प्रचार में बौद्ध संघों ने बड़ा योगदान दिया। संघ के भि्षु तथा भिक्षुणियों ने बड़ा योगदान किया।
बड़े-बड़े सम्राटों, राजाओं, सेठ-साहुकारों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार।किया और इसके प्रचार में हाथ बँटाया। मगध के राजा बिम्बिसार, कोशल नरेश प्रसेनजीत , अवन्ति के राजा प्रद्यौत ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। बुद्ध ने अपना उपदेश लोकभाषा पालि में दिया। बौद्ध संघ के भिक्षुओं ने भी इसी भाषा में उपदेश दिए। सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कदम उठाए। इन्हीं वजहों से भारत में बौद्ध धर्म का उत्यान हुआ।
साथ ही भारत में बौद्ध धर्म के पतन के भी कुछ कारण थे।
प्रथम:-
कालान्तर में बौद्ध विहारों में भिक्षु-भिक्षुणियों की चारित्रिक पवित्रता नष्ट होने के कारण उनके प्रचार कार्य में शियिलता आ गई।
द्वितीय :-
प्रारंभ में बौद्ध धर्म बड़ा सरल था । किन्तु, धीरे धीरे इसमें भी अनेक जटिल कर्म-काण्ड आ गए। बौद्ध प्रतिमाओं की पूजा होने लगी तथा विधि-विधानों पर विशेष बल दिया जाने लगा।
तृतीय:-
बौद्ध भिक्षु धार्मिक सिद्धान्तों को लेकर आपस में।लड़ने लगे और एक-दूसरे का विरोध करने लगे। बौद्ध साहित्य की संख्या भी बढ़ने लगी तथा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक जटिल समस्या बन गई कि वे किन-किन आदर्शों।का अनुसरण करें।
चतुर्थ :-
कालान्तर में बौद्ध धर्म को राजा-महाराजाओं का संरक्षण नहीं मिला। शुंग, कण्व, आंध्र- सातवाहन, गुप्त सम्राटों आदि ने बौद्ध धर्म-प्रचार के लिए कोई कदम नहीं उठाये।
पंचम:-
बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश से अनेक कुरीतियों का जन्म हुआ।
बौद्ध विहारों का शुद्ध वातावरण दूषित हो गया।
षष्ठ:-
जब उत्तर भारत में राजनीतिक एकता लुप्त होने लगी तो मुसलमानों का आक्रमण हो गया आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया।
फिर भी यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता संस्कृति, चिन्तन, सामाजिक गंठन आदि को काफी प्रभावित किया है। बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनने लगीं और.उनकी पूजा की जाने लगी। इनके अनुकरण में हिन्दु देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बना.जाने लगीं। यज्ञ के लिए मंदिर बनाए जाने लगे । इस प्रकार, मूर्तिपूजा हिन्दु धर्म का अभिन्न अंग बन गई। तत्कालीन लोकभाषापालि में अपने उपदेश देकर गौतम ने लोकभाषा के उत्थान का बुद्ध ने।रास्ता खोल दिया। अहिंसा परअतिशय बल देकर बौद्धधर्म ने भारत की राष्ट्रीय प्रकृति को
शांतिप्रिय बनाने में बड़ा योगदान किया है। बुद्ध ने धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्र चिंतन एवं तर्क पर जोर दिया। इससे धर्म एवं दर्शन के।क्षेत्र में स्वतंत्र चिन्तन को प्रोत्साहन मिला। चीन, बर्मा, सिंहल आदि अनेक दक्षिण-पूर्वी एसियाई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। विदेशों से भी अनेक छात्र और जिज्ञासु विद्वान् भारत आते थे। बोध धर्म ईश्वर और आत्मा को नही मानता है।
बौद्ध धर्म संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कारण-कार्य संबंध देखता है जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं।
बौद्ध दर्शन इस संसार को नित्य न मानकर क्षणभंगुर मानता है । उसके अनुसार वस्तुएं परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है
बौद्ध धर्म प्रत्येक जाति को समान रूउ से देखता है।
महात्मा बुद्ध कर्मकाण्ड, यज्ञ तथा पशुबलि के।घोर विरोधो धे।
महात्मा बुद्ध वेदों में विश्वास नहीं करते थे । वे अहिंसा को अपना परम धर्म मानते थे । बुद्ध मध्यम मार्ग के समर्थक थे।
बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख अंग थे- बुद्ध, संघ और धर्म ।
बौद्ध धर्म कनिष्क के समय दो भागों में विभक्त
हो गया -हीनयान तथा महायान ।
बाद में बौद्ध धर्म की एक तीसरां शाखा वज्रयान
का भी विकास हुआ। बोद्ध य्ंथ मुख्यतः पालि में पाये जाते हैं, लेकिन महायान सम्प्रदाय के ग्रथ संस्कृत में हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म का बिवरण प्रस्तुत करती हैं। इनमें तुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है।
दीपवंश एवं महावंश पालि में श्रीलंका में लिखे गये। इनमें तत्कालीन भारत के सामाजिक,।धार्मिक व आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है ।
बौद्ध धर्म के सर्वप्रमुख ग्रंथ पिटक हैं । इनको।तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-
(i) सुत्त पिटक–बुद्ध के वचन
(ii) विनय पिटक–संघ के नियम
(iil) अधिनियम पिटक-धर्म का दार्शनिक विवेचन
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई० पू० में कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में हुई। बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म रो संबंधित प्रश्नों पर उठे विवादों के निवारण के लिए संगीतियों का आयोजन किया गया ।
द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया तथा एक नया संप्रदाय महासंधिक बना लिया। शेष बौद्ध भिक्षुक थेरावादी कहलाए । बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ।आये, जहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण संन्यासियों को अपना उपदेश दिया जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्नन के नाम से जाना जाता है बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कोशल, वेशाली, कौशाम्बी एवं अन्य अनेक राज्यों में दिए। ‘प्रतीत्य समुत्पाद’ ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी शिक्षाओं का आधारस्तम्भ है ।
संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुःख का सामूहिक नाम है ‘जरामरण’। जरामरण के चक्र में बारह क्रम हैं-
(1) जरामरण (2) जाति (3) भव (4) उत्पादन (5) तृष्णा (6) वेदना (7) स्पर्श (8)।षडायतन (9) नामरूप (10) विज्ञान (11) संस्कार (12) अविद्या।
बौद्ध संघ में अल्पायु, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास आदि का प्रवेश।वर्जित था।
अपने प्रिय शिष्य आनन्द के अनुरोध पर बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। बुद्ध की प्रथम शिष्या उनकी सौतेली माँ ‘प्रजापति गौतमी’ थीं।
बुद्ध के अनुयायी मुख्यतः तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान (महायानी) तथा श्रीलंजा, बर्मा, जावा (हीनयानी) आदि देशों में फैले हुए हैं।
◆◆◆ दस शील ◆◆◆
बुद्ध ने नैतिक आचरण को शुद्ध एवं समुन्रत करने पर विशेष बल दिया। इसके लिए उन्होंने दस शील के उपदेश दिए।
वे दस शील हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह ( संग्रह न करना), बह्मचर्य, नृत्य-संगीत का त्याग, सुगंधित व श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन, कोमल शय्या का त्याग एवं कामिनी-कंचन का त्याग।
इनमें प्रथम पाँच गृहस्थों के लिए आवश्यक थे, परन्तु संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के लिए सबका पालन अनिवार्य था।
बुद्ध. ने संसार में अपना संदेश फैलाकर मानवता को दुःख, शोक, मृत्यु. भय आदि से मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक मगध, सारनाथ आदि प्रदे्शों में घूम-घूम कर शिक्षा का प्रचार किया। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ई० पू० में कुशीनगर ( गोरखपुर ) में उनका देहान्त गया। यह घटना ‘महा-परिनिर्वाण‘ कहलाती है।
यह दिलचस्प बात है कि (भारत में बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन भी हुआ। बुद्ध के उपदेश बहुत ही सरल थे। जीवन-संबंधी उनके दर्शन साधारण नियमों पर आधारित थे । ये सभी नियम युक्ति संगत एवं तर्क संगत थे। शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए सच्चरित्रता और सदाचार पर बल दिया गया। बुद्ध का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनका हदय संसार के सभी दुःखी प्राणियों के लिए संवेदना एवं करुणा से परिपूरित था। बौद्ध धर्म प्रचार में बौद्ध संघों ने बड़ा योगदान दिया। संघ के भि्षु तथा भिक्षुणियों ने बड़ा योगदान किया।
बड़े-बड़े सम्राटों, राजाओं, सेठ-साहुकारों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार।किया और इसके प्रचार में हाथ बँटाया। मगध के राजा बिम्बिसार, कोशल नरेश प्रसेनजीत , अवन्ति के राजा प्रद्यौत ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। बुद्ध ने अपना उपदेश लोकभाषा पालि में दिया। बौद्ध संघ के भिक्षुओं ने भी इसी भाषा में उपदेश दिए। सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कदम उठाए। इन्हीं वजहों से भारत में बौद्ध धर्म का उत्यान हुआ।
साथ ही भारत में बौद्ध धर्म के पतन के भी कुछ कारण थे।
प्रथम:-
कालान्तर में बौद्ध विहारों में भिक्षु-भिक्षुणियों की चारित्रिक पवित्रता नष्ट होने के कारण उनके प्रचार कार्य में शियिलता आ गई।
द्वितीय :-
प्रारंभ में बौद्ध धर्म बड़ा सरल था । किन्तु, धीरे धीरे इसमें भी अनेक जटिल कर्म-काण्ड आ गए। बौद्ध प्रतिमाओं की पूजा होने लगी तथा विधि-विधानों पर विशेष बल दिया जाने लगा।
तृतीय:-
बौद्ध भिक्षु धार्मिक सिद्धान्तों को लेकर आपस में।लड़ने लगे और एक-दूसरे का विरोध करने लगे। बौद्ध साहित्य की संख्या भी बढ़ने लगी तथा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक जटिल समस्या बन गई कि वे किन-किन आदर्शों।का अनुसरण करें।
चतुर्थ :-
कालान्तर में बौद्ध धर्म को राजा-महाराजाओं का संरक्षण नहीं मिला। शुंग, कण्व, आंध्र- सातवाहन, गुप्त सम्राटों आदि ने बौद्ध धर्म-प्रचार के लिए कोई कदम नहीं उठाये।
पंचम:-
बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश से अनेक कुरीतियों का जन्म हुआ। बौद्ध विहारों का शुद्ध वातावरण दूषित हो गया।
षष्ठ:–
जब उत्तर भारत में राजनीतिक एकता लुप्त होने लगी तो मुसलमानों का आक्रमण हो गया आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया।
◆◆◆◆◆
फिर भी यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता संस्कृति, चिन्तन, सामाजिक गंठन आदि को काफी प्रभावित किया है। बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनने लगीं और.उनकी पूजा की जाने लगी। इनके अनुकरण में हिन्दु देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बना.जाने लगीं। यज्ञ के लिए मंदिर बनाए जाने लगे । इस प्रकार, मूर्तिपूजा हिन्दु धर्म का अभिन्न अंग बन गई। तत्कालीन लोकभाषापालि में अपने उपदेश देकर गौतम ने लोकभाषा के उत्थान का बुद्ध ने।रास्ता खोल दिया। अहिंसा परअतिशय बल देकर बौद्धधर्म ने भारत की राष्ट्रीय प्रकृति को शांतिप्रिय बनाने में बड़ा योगदान किया है। बुद्ध ने धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्र चिंतन एवं तर्क पर जोर दिया। इससे धर्म एवं दर्शन के।क्षेत्र में स्वतंत्र चिन्तन को प्रोत्साहन मिला। चीन, बर्मा, सिंहल आदि अनेक दक्षिण-पूर्वी एसियाई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। विदेशों से भी अनेक छात्र और जिज्ञासु विद्वान् भारत आते थे। बोध धर्म ईश्वर और आत्मा को नही मानता है।
बौद्ध धर्म संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कारण-कार्य संबंध देखता है जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। बौद्ध दर्शन इस संसार को नित्य न मानकर क्षणभंगुर मानता है । उसके अनुसार वस्तुएं परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है।
बौद्ध धर्म प्रत्येक जाति को समान रूउ से देखता है।
महात्मा बुद्ध कर्मकाण्ड, यज्ञ तथा पशुबलि के।घोर विरोधो धे।
महात्मा बुद्ध वेदों में विश्वास नहीं करते थे । वे अहिंसा को अपना परम धर्म मानते थे । बुद्ध मध्यम मार्ग के समर्थक थे।
बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख अंग थे- बुद्ध, संघ और धर्म ।
बौद्ध धर्म कनिष्क के समय दो भागों में विभक्त
हो गया -हीनयान तथा महायान ।
बाद में बौद्ध धर्म की एक तीसरां शाखा वज्रयान
का भी विकास हुआ। बोद्ध य्ंथ मुख्यतः पालि में पाये जाते हैं, लेकिन
महायान सम्प्रदाय के ग्रथ संस्कृत में हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म का बिवरण प्रस्तुत करती हैं। इनमें बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन मीलता है।
दीपवंश एवं महावंश पालि में श्रीलंका में लिखे गये। इनमें तत्कालीन भारत के सामाजिक,।धार्मिक व आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है ।
बौद्ध धर्म के सर्वप्रमुख ग्रंथ पिटक हैं । इनको।तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-
(i) सुत्त पिटक–बुद्ध के वचन
(ii) विनय पिटक–संघ के नियम
(iil) अधिनियम पिटक-धर्म का दार्शनिक विवेचन
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई० पू० में कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में हुई। बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म रो संबंधित प्रश्नों पर उठे विवादों के निवारण के लिए संगीतियों का आयोजन किया गया ।
द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया तथा एक नया संप्रदाय महासंधिक बना लिया। शेष बौद्ध भिक्षुक थेरावादी कहलाए । बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ।आये, जहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण संन्यासियों को अपना उपदेश दिया जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्नन के नाम से जाना जाता है बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कोशल, वेशाली, कौशाम्बी एवं अन्य अनेक राज्यों में दिए। ‘प्रतीत्य समुत्पाद’ ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी शिक्षाओं का आधारस्तम्भ है ।
संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुःख का सामूहिक नाम है ‘जरामरण’। जरामरण के चक्र में बारह क्रम हैं-
(1) जरामरण (2) जाति (3) भव (4) उत्पादन (5) तृष्णा (6) वेदना (7) स्पर्श (8) षडायतन (9) नामरूप (10) विज्ञान (11) संस्कार (12) अविद्या।
बौद्ध संघ में अल्पायु, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास आदि का प्रवेश।वर्जित था।
अपने प्रिय शिष्य आनन्द के अनुरोध पर बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। बुद्ध की प्रथम शिष्या उनकी सौतेली माँ ‘प्रजापति गौतमी’ थीं।
बुद्ध के अनुयायी मुख्यतः तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान (महायानी) तथा श्रीलंजा, बर्मा, जावा (हीनयानी) आदि देशों में फैले हुए हैं।

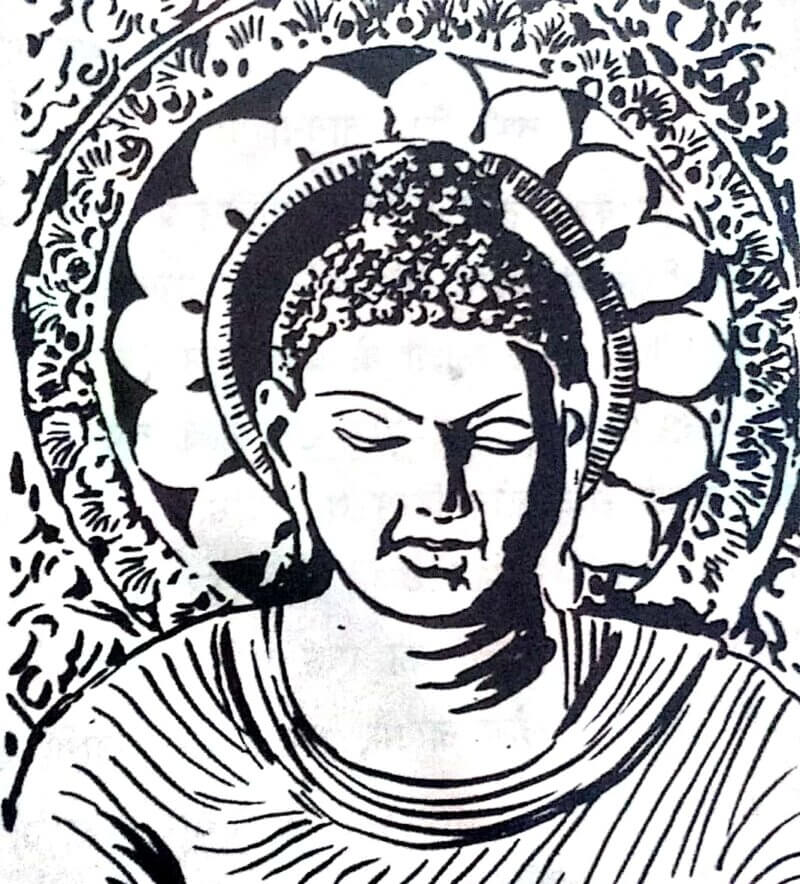
great information